हिंदी साहित्य के इतिहास को कई महत्वपूर्ण काल में विभाजित किया गया है और इस वर्गीकरण में भक्ति काल (Bhakti Kaal) का द्वितीय स्थान रहा है।
Bhakti Kaal तेरहवीं से सौलवीं शताब्दी के बीच का काल रहा है, जिसके दौरान हिंदी साहित्य के महान लेखक और कवी जैसे कालिदास, संत कबीर, जायसी, तुलसीदास आदि जिन्होंने उस काल में अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति को चरम सीमा पर पहुंचाया। इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग कहा जाता है।
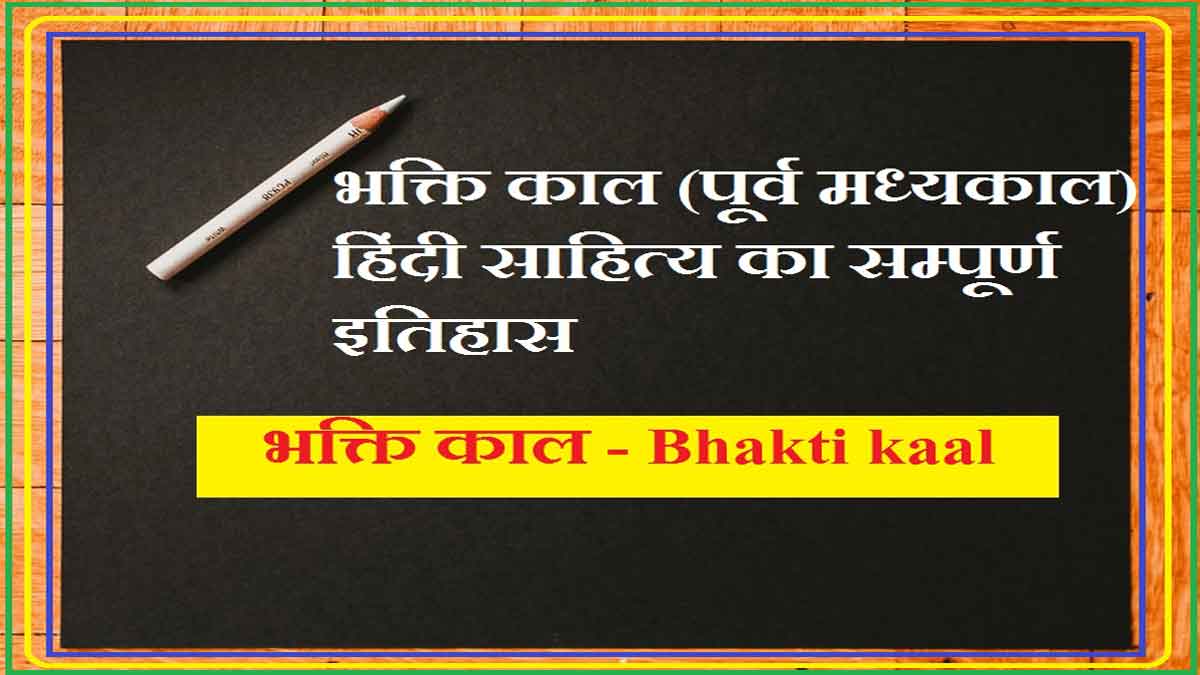
यहां भक्ति काल क्या है (bhakti kaal kya hai), भक्ति काल किसे कहते हैं, भक्ति काल की परिभाषा, भक्तिकाल का नामकरण, भक्तिकाल के कवि, भक्तिकाल का विभाजन, भक्ति काल की शाखाएं, भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल का समय आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे।
भक्ति काल क्या है?
14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अखिल भारतीय स्तर पर जिस विराट चिंतन धारा का प्रभाव रहा, उसे ही भक्ति के नाम से जाना जाता है और वही काल भक्ति काल कहलाता है।
भक्ति काल किसे कहते हैं?
हिंदी साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के युग को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है।
इस दौर में मुख्य रूप से भक्ति विषयक काव्य रचे गए। इस दौर में भक्ति काव्य की निर्मित लंबी परंपरा रही, जिसमें हुए कवियों ने धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विशेषता रखने वाली कई कविताओं की रचना की।
भक्ति काल का अर्थ
भक्ति काल उस दौर को कहा जाता है जब समकालीन कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण की कविता लिखी।
अगर भक्ति काल का संधि विच्छेद करें तो भक्ति+काल होता है। भक्ति भज धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवा करना एवं काल का अर्थ होता है समय। इस तरह भक्ति काल का अर्थ वह समय जब भगवान की भक्ति और समर्पण का भाव जाग्रत हुआ था।
भक्तिकाल का उदय
भक्ति आंदोलन के उदय के कारण के पीछे अलग-अलग हिंदी साहित्य के विद्वानों का अलग-अलग मत हैं।
वैसे भक्ति आंदोलन के उदय पर सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लेखक ग्रियर्सन ने विचार किया है और उनके अनुसार इस आंदोलन के उदय दो तरह से हुआ है।
पहला यह एक अचानक पैदा होने वाला आंदोलन है, जो बिजली की चमक के सामान फेल गया। दूसरा इन्होंने इसे ईसाई प्रभाव से भी जोड़ा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे मुस्लिम राज्य व्यवस्था की स्थापना का कारण जोड़ा है।
उनके अनुसार उस समय तक पूरे भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था, जिसके कारण पौरुष से हताश जाति के लोग भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था।
इसी के कारण इस आंदोलन ने जन्म लिया ताकि दोबारा लोगों में भगवान के प्रति आस्था, प्रेम और समर्पण का भाव उत्पन्न किया जा सके।
हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के इन विचारों पर असहमति जताते हुए कहा है कि यदि भक्ति आंदोलन का उदय भारत में मुसलमानों के अत्याचार से होना था तो इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले सिंध या उत्तर भारत में होना चाहिए था।
क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना उत्तर भारत से ही हुई और सबसे ज्यादा मुस्लिम साम्राज्य का राज्य उत्तर भारत में ही था। लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, जो रामचंद्र शुक्ल के विचारों को गलत साबित करता है।
उनके अनुसार भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण भारत से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में जगाई।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रियर्सन के विचारों का भी खंडन किया और उन्होंने कहा कि अचानक बिजली के चमक के सामान धार्मिक मतों का फैलाना यह सत्य नहीं है। क्योंकि भक्ति आंदोलन फैलने के पीछे सैकड़ों वर्ष का संघर्ष रहा है और सैकड़ों लोगों ने अपना योगदान दिया है।
वहीं डॉ. रामविलास शर्मा व्यापार के विकास व सामाजिक संरचना के विखंडन को भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण मानते हैं।
भक्ति काल का नामकरण
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तित्व की प्रधानता के आधार पर ही पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नामकरण किया है।
रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इस युग की कविताओं की मूल संवेदना भक्ति रही है चाहे राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो या संत काव्य। सभी में मूल केंद्र भक्ति ही रहा है। इस तरह भक्ति के स्वरूप में भीन्नता नजर आती है लेकिन केंद्र बिंदु भक्ति ही है।
हालांकि इस युग में कई वीरगाथा और अन्य तरह की गीते भी लिखी गई, लेकिन अन्य रचनाओं की तुलना में भक्ति परक रचनाओं की संख्या ज्यादा है। अतः पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल (bhaktikaal) कहना उचित माना गया है।
भक्ति काल की समय सीमा
भक्ति काल की समयावधि 1350 से 1650 ईसवीं तक मानी जाती है। वैसे भक्ति काल के आरंभ को लेकर विद्वानों में मतभेद चलता रहा है। अधिकांश विद्वान भक्ति काल का आरंभ 1350 ईस्वी से मानते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का आरंभ 1375 ईस्वी से हुआ है।
भक्ति काल का इतिहास
भक्ति काल का इतिहास छठी शताब्दी से है। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज और हिंदू धर्म में सुधार तथा इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच समन्वय स्थापित करना था।
छठी शताब्दी में इसका उदय दक्षिण भारत से हुई और इसकी शुरुआत अलवार और नयनार संतों ने की। अलवार और नयनार विष्णु और शिव के भक्त थे।
धीरे-धीरे रामानंद के द्वारा यह आंदोलन 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में भी फैला। अलवर और नयनार संतो के द्वारा शुरु की गई भक्ति के इस आंदोलन में ऊंच- नींच, जाति, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं था।
788 से 820 ईसवी तक शंकराचार्य ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। हालांकि वे दूसरी ओर ब्राह्मण और जीव के बीच भेद नहीं करते थे। वैसे शंकराचार्य शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने के लायक नहीं समझा करते थे।
भक्ति काल की शाखाएं
भक्ति काल में कुल 4 शाखाएं थी:
- ज्ञानाश्रयी शाखा
- प्रेमाश्रयी शाखा
- रामाश्रयी शाखा
- कृष्णाश्रयी शाखा
ज्ञानाश्रयी शाखा
भक्ति काल में जिन कवियों ने ईश्वर के निराकार स्वरूप को अपनाकर ज्ञान मार्ग से ईश्वर को अनुभव किया है, उन्हीं को ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है।
ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने अपने कविताओं में हमेशा ही गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे वैयक्तिक साधना पर बल देते थे।
ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जाती पाती का हमेशा ही विरोध किए हैं। वे मिथ्या आडंबर और रूडियो का असमर्थन करते थे। इनकी रचना में कई बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है।
इसीलिए इनकी काव्य भाषा को साधु ककड़ी कहा गया है। कबीर दास, रैदास, नानक, मलूकदास, सुंदर दास और दादू दयाल ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं।
प्रेमाश्रयी शाखा
भक्ति काल में मुसलमान सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से जाना जाता है।
यह शाखा का नाम होने का कारण है कि सूफी कवि मानते थे ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम प्रेम है। क्योंकि ईश्वर का जीवों के साथ प्रेम का ही संबंध होता है।
यही कारण है कि मुसलमान सूफी संतों ने कई प्रेमगाथा ही लिखी है। जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत प्रमुख है। मंझन, कुतुबन और उसमान प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं।
मुसलमान सूफी कवियों के द्वारा लिखी गई प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली में रची गई है। इनकी भाषा अवधि रही है। इन्होंने भी दोहा, छंद, चौपाई का प्रयोग किया है।
सूफी कवि भी खंडन मंडल में ना पड़कर भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्रेम का वर्णन किया है। इन्होंने एक मुसलमान होते हुए हिंदू जीवन से संबंधित कई कथाएं लिखी हैं।
रामाश्रयी शाखा
सगुण काव्य धारा में जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार को राम के रूप में पूजा है, उन्हें रामाश्रय शाखा के कवि कहा जाता है। रामाश्रय कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है।
रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास और नरहरी दास आदि का नाम आता है।
दस्य भाव की भक्ति, मर्यादावाद, मानवतावाद, राम का लोकनायक रूप, लोकमंगल की सिद्धि, लोक कल्याण की भावना, मर्यादा और आदर्श की स्थापना, दार्शनिक प्रतीकों की बहुलता रामाश्रय शाखा की विशेषता रही है।
लेकिन इन कवियों में तुलसीदास को रामाश्रय शाखा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि माना जाता है, जिनकी रचना राम चरित्र मानस विश्व प्रसिद्ध है।
कृष्णाश्रयी शाखा
भक्ति काल में जिन कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार रूप को कृष्ण के रूप में पूजा उनकी उपासना कि उन्हें कृष्णा सही शाखा का कवि माना जाता है।
भक्ति काल में ब्रज मंडल में कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत ही उत्साह और उल्लास के भावना के साथ हुआ। इस दौरान कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय सक्रिय हुए, जिनमें राधावल्लभ, हरिदास, निंबार्क और चैतन्य संप्रदाय उल्लेखनीय है।
कृष्णा श्री शाखा का आधार ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत को माना जाता है। इस शाखा के प्रवर्तन का श्रेय हिंदी में विद्यापति को दिया जाता है।
ब्रज भाषा में भ्रमरगीत परंपरा का श्रेय सूरदास को जाता है, जिन्होंने इस परंपरा का प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन में केवल कृष्णाश्रय शाखा के कवियों के काव्य में ही नारी मुक्ति का स्वर देखने को मिलता है।
सामान्यता पर बल, नारी मुक्ति श्रृंगार चित्रण, कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण, बाल लीला एवं वात्सल्य वर्णन, काव्य, भाषा और ब्रजभाषा, लोक संग्रह, आश्रित्व का विरोध, कृष्णाश्रयी शाखा के काव्य की विशेषता रही है।
हिन्दी की प्रमुख गद्य रचनाएँ एवं रचयिता आदि के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।
भक्ति काल के प्रकार
भक्ति काल को दो भागों में बाटा गया है:
- निर्गुण काव्यधारा
- सगुण काव्यधारा
निर्गुण और सगुण काव्य धारा के भी दो-दो भेद हैं।
| निर्गुण काव्य धारा के भेद | सगुण काव्यधारा के भेद |
|---|---|
| सन्त काव्य धारा | राम काव्य धारा |
| सूफी काव्यधारा | कृष्ण काव्य धारा |
निर्गुण काव्यधारा
निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति है, जिसमें ईश्वर के रूप, रंग और आकार की कल्पना नहीं की गई है। भक्त अपने ज्ञान शक्ति से ईश्वर की कल्पना कर सकता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर के हर जगह वास होना बताया गया है।
निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्गी है और इस ज्ञान मार्ग पर गुरु के मार्गदर्शन से ही चल सकते हैं। निर्गुण भक्ति में मस्जिद, रोजा मंदिर, तीर्थ माला, नमाज, जपमाला जैसे आडंबर का विरोध किया गया है।
निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। निर्गुण भक्ति में जाती, पाती, वर्ण, भेद और छुआछूत का कोई स्थान नहीं है।
इसमें सभी भक्तजन एक समान है। निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं है।
सगुण भक्ति काव्य धारा
जो ईश्वर की मूर्त या साकार रूप की भक्ति करता है, उसे सगुण भक्ति कहा जाता है। इस तरह सगुण भक्ति में ईश्वर की रंग, रूप, गुण, जाति होती है। इसमें मूर्ति पूजा, जप तप, तीर्थ यात्रा, नित्यध्यान सब चीजों की आवश्यकता बताई गई है।
हालांकि सगुण भक्ति में भी गुरु की महिमा को अनंत बताया गया है। सगुण भक्ति में ईश्वर के अलग-अलग रूपों को बताया गया है। साथ ही इसमें नए अवतार का भी वर्णन किया गया है।
इस तरह सगुण भक्ति ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करता है। तुलसीदास, मीरा, रसखान, सूरदास सभी सगुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं।
भक्ति काल के प्रमुख कवि
भक्ति काल में कई कवि हुए। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रमुख भक्ति काल के कवि इस प्रकार है:
कबीरदास, कृष्णदास, रहीमदास, परमानंद दास, कुंभनदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, मीराबाई, स्वामी हरिदास, व्यास जी, रसखान, मदनमोहन, श्रीभट्ट, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु।
भक्ति काल के कवियों का विभाजन
भक्ति काल के कवियों को निर्गुण काव्य धारा व सगुण काव्य धारा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है।
निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि
रैदास
रैदास जिनका असल नाम रविदास था। इन्हें निर्गुण ज्ञानश्री काव्यधारा का प्रमुख कवि माना जाता है। इनका जन्म 1398 ईसवी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था।
इनके माता का नाम कर्मा देवी और पिता का नाम संतोष दास था। यह रामानंद जी के शिष्य थे। रैदास की रचनाएं संतमन के विभिन्न संग्रह में संकलित है।
रैदास ने अपने दोहे और पदों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया।
संत रविदास जी (रैदास) का जीवन परिचय विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।
कबीरदास
कबीर दास को निर्गुण शाखा के ज्ञानश्री काव्य धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। इनका जन्म 1398 ईसवी में हुआ था।
वैसे इनके असल माता-पिता के बारे में नहीं पता लेकिन इनका लालन-पालन नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे दंपतियों ने किया था। कबीर दास के गुरु का नाम रामनंद था। कबीर दास की मृत्यु 1528 में हुई थी।
कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लुई था। जिससे इनके दो बच्चे हुए, जिसका नाम कमाल और कमाली रखा गया था।
कबीर दास राम भक्त थे लेकिन भगवान राम को निर्गुण निराकार मानते थे। कबीर दास ने सदा ही अपनी रचना से अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जात पात, माया छुआछूत का उग्र विरोध किया है। इनकी रचनाएं बीजक नाम से संग्रहित है। जिसके 3 भाग है साखी, शबद और रमेणी।
कबीर दास का जीवन परिचय विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।
गुरु नानक देव
निर्गुण ज्ञानश्री काव्य धारा के प्रमुख कवियों में गुरु नानक देव जी का भी नाम आता है, जिनका जन्म 1469 में पंजाब राज्य के ननकाना साहिब के तलवारी नामक गांव में हुआ था।
गुरु नानक जी को सिखों के प्रथम गुरु माना जाता है। इनके पिता का नाम कालू चंद एवं माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं रहिरास, आसा दी वार, जपुजी और सोहिला है।
इन्होंने कई पद, भजन और साखियां लिखी, जिसे सन 1604 में सिखों के छठे गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया। गुरु नानक जी की मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी।
मलूक दास
मलूक दास निर्गुण ज्ञानश्री काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। इनका जन्म 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के कडा नामक गांव में हुआ था।
इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें प्रमुख रचनाएं पुरुष विलास, गुरु प्रताप अलखवनी, ज्ञानबोध, रतनखान, भक्तिविवेक, अवतार लीला, बारहखड़ी, भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, ब्रजलीला और ध्रुवचरित है। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी।
सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि
गोस्वामी तुलसीदास
गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्ति काव्य धारा का प्रमुख कवि माना जाता है, जिनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था।
कहा जाता है मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता-पिता ने इनका परित्याग कर दिया था।
तुलसीदास ने संपूर्ण जीवन काल राम भक्ति में लीन रहकर कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें रामचरित मानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनयपत्रिका, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, रामलला नहछू, बरवै रामायण, बैराग्य सन्दीपनी, कवितावली आदि शामिल है।
तुलसीदास की तमाम रचनाओं में राम चरित्र मानस को प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना इन्होंने 1574 में की थी और इसे लिखने में इन्हें 2 वर्ष 9 माह का समय लगा था।
इस ग्रंथ को इन्होंने अलग-अलग कांड में विभाजित किया है जैसे बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड।
गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।
स्वामी रामानन्द
राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि स्वामी रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। इनका जन्म 1400 ईसवीं में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु 1470 ईस्वी में हुई थी।
इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ “श्री रामानुजन पद्धति” और “वैष्णव मताब्द भास्कर” है। इन्होंने हनुमान जी की प्रसिद्ध स्तुति भी लिखी है, जो इस प्रकार है “आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की”।
रामानंद जी के विचारधारा से स्वयं गोस्वामी तुलसीदास भी प्रभावित थे। रामानंद जी भक्ति मार्ग में सभी वर्ग के भक्तों को समान मानते थे। जिसके कारण इनके शिष्य अलग-अलग वर्ग के थे, जिसमें कबीर दास, धन्ना, पीपा और रैदास आदि हैं।
स्वामी अग्रदास
स्वामी अग्रदास को भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों की सूची में गिना जाता है। इनके गुरु कृष्णदास पयहरी थे, जिनसे इन्होंने दीक्षा लेकर शिष्यत्व प्राप्त किया था।
‘रामभजन मंजरी’, ‘उपासना बावनी’,’ध्यान मंजरी’, ‘हितोपदेश उपखाणाँ बावनी,’ और ‘कुंडलिया’ आदि इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है।
नाभादास
राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में नाभादास का भी नाम आता है, जो अग्रदास के शिष्य थे।
ये तुलसीदास के समकालीन थे और उनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं अष्टयाम, भक्तमाल और राम भक्ति। अष्टयाम में सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का इन्होंने चित्रण किया है।
ईश्वरदास
ईश्वरदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है, जिनकी सुप्रसिद्ध कृति सत्यवती है, जिसकी रचना इन्होंने 1501 ईसवी में की थी।
इसके अतिरिक्त रामकथा से संबंधित इनका “अंगद पेर” और “भरत मिलाप” दो रचनाएं काफी प्रचलित है। भरत मिलाप में इन्होंने भरत और भगवान राम दो भाइयों के मिलन की करुण कोमल प्रसंग का वर्णन किया है।
वहीं अंगद पेज में उन्होंने रावण की सभा में अंगद के पैर जमा कर डट जाने का वीर रस से परिपूर्ण प्रसंग का वर्णन किया है। ईश्वरदास का जन्म 1480 ईस्वी में माना जाता है।
केशवदास
केशव चंद हिंदी साहित्य और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है, जिन्होंने विज्ञान गीता, कविप्रिया, रसिकप्रिया,जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, वीरसिंहचरित और रतनबावनी आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की। इनका जन्म 1554 में हुआ था और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी।
भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएँ आदि के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।
भक्तिकाल की परिस्थितियाँ
राजनैतिक परिस्थितियाँ
भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईसवी का दौर युद्ध, अशांति और संघर्ष का समय था। इस काल में मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर शाहजहां तक का शासन रहा।
इस समय तक उत्तरीभारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और इन दिनों मुस्लिम और अफ़गानों के बीच काफी संघर्ष चल रहे थे, जो चारों तरफ अशांति फैला रही थी।
इस कालखंड में दिल्ली पर तुगलक वंश, लोधी वंश, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे कई मुगल शासकों ने शासन किया। मुगल काल राजनीतिक दृष्टि से काफी अशांत और संघर्ष में रहा। इस समय तक समाज में कई कुर्तियां फैल चुकी थी।
हालांकि मुगल वंश के बादशाह काव्य और कला प्रेमी हुआ करते थे। लेकिन निरंतर युद्ध और अव्यवस्थित शासन व्यवस्था इसके साथ ही पारिवारिक कलहो ने देश में अशांति फैला रखी थी।
सामाजिक परिस्थितियाँ
भक्ति काल के 15 वी शताब्दी के दौरान समाज पूरी तरीके से कुप्रथा को झेल रहा था। इस समय हिंदू समाज की स्थिति बहुत ही सोचनीय थी।
समाज में जाति पाती जैसे कई विचारधाराएं फैल चुकी थी। मुस्लिम स्वार्थवश हिंदूओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। हिंदू कन्याओं से जबरन विवाह कर लेते थे।
अमीर लोग कुलीन नारियों का अपहरण करा रहे थे। जिसके कारण ऐसी नारियों को बचाने के लिए हिंदू जनता ने बाल विवाह और पर्दा प्रथा का नियम शुरू कर दिया। इस कुप्रथा ने मानो औरत के अस्तित्व को ही छीन लिया।
इस दौर में संत कबीर दास ने अपनी रचनाओं से जाती पाती के भेदभाव और अंध श्रद्धा का प्रखर विरोध किया। आगे चलकर मुस्लिम शासकों में सद्भाव और सहिष्णुता के भाग जागे। हिंदू और मुसलमानों के बीच सामंजस्य स्थापित होने लगा।
धार्मिक परिस्थितियाँ
भक्ति काल के उस दौर में धार्मिक परिस्थितियां समाज में बहुत ही बड़ी सोचने का विषय बन चुका था। क्योंकि उस समय समाज में विविध धर्मों और संप्रदायों में जन्म ले लिया था और उन धर्मों में आपसी में कोई समन्वय की भावना या प्रेम नहीं थी।
हर कोई अपने अपने धर्म को मजबूत करने पर लगा हुआ था फिर चाहे समाज में लोगों के बीच अशांति ही क्यों ना फैले। उन्हें अपने धर्म को सर्वोपरि बनाने से मतलब था।
एक ओर वैष्णव धर्म अपनी परंपरा की जड़े मजबूत कर रहा था तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म का विकृत रूप उभर कर आ रहा था। सूफी धर्म के लोग भी अपने जड़े मजबूत करने में लगे हुए थे।
गोरखनाथ प्रमुख रहे जिन्होंने नाथ संप्रदाय को चलाएं और अपनी संप्रदाय को मजबूत स्थिति बनाने में लगे हुए थे।
इस तरह उस समय समाज में कई संप्रदाय थे, जिन्होंने आपसी मेल मिलाव और एकता को छोड़ अलग-अलग मार्ग अपना लिए थे।
साहित्यिक परिस्थितियाँ
भक्ति काल में हुए कवियों ने अपने विचारों को गद्य में ना व्यक्त करते हुए उसे छंद-बद्ध रूप में व्यक्त किया। उस समय निर्गुण साधना पद्धति और सगुण साधना पद्धति को इस काल के साहित्य में देखा गया।
हिंदू कवियों के साथ-साथ मुसलमान कवियों ने भी इस साहित्य धारा में भाग लिया और उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति विषयक रचना की, जिसने दोनों संप्रदाय को एक करने का प्रयास किया।
कुछ कवियों ने कर्मकांड, ऊंच-नीच का विरोध करते हुए आपसी द्वेष को दूर करने का प्रयास किया तो कुछ ने प्रेम पीर के माध्यम से दोनों संप्रदाय को निकट लाने की कोशिश की।
इस काल का साहित्य अपनी विविधता के कारण ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल साबित हुआ।
भक्तिकाल की विशेषताएं
भक्ति काल (bhakti kaal) भले निर्गुण और सगुण दो भागों में विभाजित हो गई लेकिन इन दोनों ही विचारधाराओं के सिद्धांत और इसके जीवन मूल्य में समानता देखने को मिली, जिसने इस युग को और भी विशिष्ट बना दिया।
इस युग के विभिन्न विचारधाराओं के कवियों की रचना में कृष्ण भक्ति, राम भक्ति देखने को मिलती है। इन्हीं समानता के कारण भक्ति काल की कुछ सामान्य विशेषता निम्नलिखित है:
भक्तिभावना की प्रधानता
भक्ति काल की पहली विशेषता भक्ति भावना की प्रधानता ही है। भक्ति काल के सभी निर्गुण और सगुण कवि और सूफी संतों ने भक्ति भावना की इस अनुभूति को गहराई से अनुभव किया है।
उन्होंने भक्ति भावना को मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया है। संपूर्ण भक्ति काल में यह भक्ति भावना का प्रवाह हुआ है।
गुरु का महत्त्व
भक्ति काल में विभिन्न धाराओं के कवियों ने अपनी रचना में गुरु की महिमा को दर्शाया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया है।
उनकी रचनाओं से पता चलता है कि गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि गुरु ही परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं।
कबीर, जायसी, तुलसीदास जैसे सभी महान संतों ने अपनी रचना में गुरु की महिमा किया है, जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है:
गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पाय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय।।
प्रेम तत्त्व का महत्त्व
भक्ति काल के कवियों की रचना में प्रेम तत्व का महत्व होना भी एक खास विशेषता है। भक्ति काल के निर्गुण और सगुण और सूफी संत ने अपनी रचना में प्रेम की महिमा और सत्ता को स्वीकार किया है। सभी संतो ने भक्ति के मार्ग को प्रेम का मार्ग बताया है।
सगुण कवियों ने प्रेम की पीड़ा को पर्याप्त महत्व देते हुए प्रेम को मानव मन की कोमलतम भावना बताई है। भक्ति काल (bhakti kal) के कवियों का मानना है कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भक्तों के हृदय में धीरे-धीरे प्रेम और श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है।
अहंकार का त्याग
भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचना में अहंकार के त्याग पर जोड़ दिया है और भक्ति काल की यह एक विशेष विशेषता रही है, जो सभी धाराओं के कवियों में देखने को मिलता है।
सभी कवियों का मानना है कि अहंकार को बिना त्यागे सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है। समर्पण भाव से ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है।
भक्ति काल के कवियों में अपनी रचनाओं में कई ऐसी पंक्तियां जोड़ी है, जो अहंकार के त्याग के महत्व को दर्शाता है। इसमें परमानंद दास जी के द्वारा लिखी एक पंक्ति इस प्रकार है, जो अहंकार के त्याग को दर्शाता।
कहा करो वऐकउंठहइ जाय।
जह नहीं नंद, जहां न जसोदा।
नहीं जो गोकुल ग्वाल न गाय।।
बहुदेववाद का विरोध
भक्ति काल के कवियों की रचना में बहूदेववाद का विरोध भी देखने को मिलता है, जो भक्ति काल की एक खास विशेषता रही है। इस काल के सगुण और निर्गुण दोनों ही कवियों ने अपनी रचना में बहुदेववाद का विरोध किया है। उन्होंने ईश्वर के एक ही रूप को माना है।
हालांकि निर्गुण कावियो ने अवतारवाद का विरोध किया है लेकिन सगुण संतों ने अवतारवाद को स्वीकारा है।
सभी कवियों ने संपूर्ण सृष्टि के लिए एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की है और जो लोग ईश्वर के अलग-अलग रूप की पूजा करते हैं, उनकी उपासना को व्यर्थ बतलाया है।
इन कवियों का मानना है कि देवताओं के विभिन्न नाम एक ही ईस्वर के विभिन्न रूप हैं। भक्ति काल में बहुदेववाद का विरोध करता हुआ एक पंक्ति उदाहरण के रूप में इस प्रकार हैं:
शिवद्रोही मम ‘कहावा।
सौ नर मोहि हूँ नहीं भावा।।
शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता
भक्ति काल की एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि इस युग के कवियों ने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा करते हुए निजी अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है।
इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है कि शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता जब तक वह व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं करता।
भक्ति काल की यह विशेषता हमें कबीर दास के द्वारा लिखी इस पंक्ति से जानने को मिलती है:
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोई।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।।
वर्गभेद का विरोध
भक्ति काल में पूरा समाज वर्ग भेद में बटा हुआ था। समाज में जाति पाति, ऊंच-नीच और छुआछूत जैसी भावनाएं लोगों में व्याप्त थी, जिसने समाज को कई टुकड़ों में बांट दिया था।
शुद्र लोगों के लिए धार्मिक कार्य निषेध था। उनकी मात्र छाया पड़ जाना ही अपवित्र माना जाता था। समाज में ऐसी ऊंच-नीच की भावना लोगों में आपस में नफरत उत्पन्न कर रही थी।
ऐसे में उस रूढ़िवादी काल में भक्ति काल के सभी कवियों ने अपनी रचना के माध्यम से वर्ग भेद का कठोरता से विरोध किया है।
भक्ति काल के कवियों ने समाज के इन भावनाओं को बुरी दृष्टि से देखा है और उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज के इन विचारधाराओं को समाप्त करने की कोशिश की है।
जिसमें कबीर दास के द्वारा लिखी गई यह पंक्ति काफी प्रचलित है:
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान।।
रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन
भक्ति काल के कवियों की रचनाओ में रुढ़िवादी विचारधारा के खंडन की विशेषता देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त बलि प्रथा, तीर्थयात्रा, मूर्ति पूजा, व्रत, रोजा जैसे आडंबरो का खुलकर विरोध किया है।
यहां तक कि सगुन भक्त कवियों ने भी कहीं-कहीं रूढ़िवादी भावनाओं का विरोध किया है। उन्होंने अपनी रचना में शालीनता, क्षमता, सद्भाव और सहजता जैसे मूल्यों को महत्व दिया है।
भक्ति काल के कवियों के द्वारा रूढ़िवादी विचारधारा को बयां करती कबीर दास की यह कविता प्रचलित है:
कबीर पाहन पूजे हरि मिलै, तो मैं पूजूं पहार।
घर की चाकी क्यों नाहिं पूजैं पीसि खाय संसार।।
शृंगार वर्णन
भक्ति काल के विभिन्न विचारधाराओं के कवियों की रचनाओ में एक समानता श्रृंगार वर्णन का भी देखने को मिलता है, जो भक्तिकाल की एक खास विशेषता है।
भक्तिकाल के कवियों ने अपनी रचना में भक्ति भावना के बावजूद श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है और ना केवल सगुन विचारधारा के लोग बल्कि निर्गुण विचारधारा के संत जो भगवान के स्वरूप को निराकार मानते हैं, उन्होंने भी अपनी रचना में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है।
हालांकि इनकी रचना में वियोग का स्वर अधिक मुखरित होता है। यहां पर तुलसीदास की एक खूबसूरत पंक्ति है, जिसमें शृंगार रस का प्रयोग किया गया है।
तिलक वियोग तिहारे मैं देखी तस जाई जानकी मनहू विरह मूरति मन को।
रसना रटति नाम कर थिर चिर रहे निज पद कमल तिहारे।।
नारी-विषयक दृष्टिकोण
भक्ति काल के कवियों की रचना में एक अच्छी विशेषता यह देखने को मिलती है कि उन्होंने नारी विषयक दृष्टिकोण को सहजता से अभिव्यक्त किया है।
भक्ति काल के कवि सामंती सोच से ऊपर उठकर पतिव्रता स्त्री के मुक्त कंठ से प्रशंसा किए हैं। वहीं कुटीर स्त्री की उन्होंने कुर्ता से निंदा भी की है।
इस तरह भक्ति काल के कवियों के रचना से प्रतीत होता है कि नारी के सत्स्व रूप पर आदरणीय दृष्टि इनकी थी, वहीं असत्य स्वरुप पर निंदा मय दृष्टि थी।
यह विशेषता भक्ति काल के कवि कबीर दास के इस रचना से देखने को मिलती है:
नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग।
कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग।।
सत्संगति की महिमा
भक्ति काल के रचना में सत्संगति की महिमा भी देखने को मिलती है। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दोनों ही विचारधारा के कवियों ने अच्छी संगति में रहने का महत्व बताया है और उसका गुणगान किया है।
भक्त कवियों का मानना था कि सत्संगति से मानव मन के दोष दूर होते हैं। सत्संगति दूसरों के कष्टों का हरण करता है।
इसीलिए भक्तिकाल के कवियों ने बुरे लोगों का साथ त्याग कर अच्छे लोगों की संगत में रहने की शिक्षा दी है और ऐसा ही भाव कबीर दास के द्वारा लिखी इस पंक्तियों से आती हैं:
कबिरा संगति साधु की हरे और की व्याधि।
संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि॥
भाषा शैली
भक्ति काल के साहित्य की एक अच्छी विशेषता भाषा शैली भी रही है। भक्तिकाल के विभिन्न विचारधाराओं के कवियों के द्वारा लिखी गई रचना में उन्होंने प्रचलित लोक भाषा का प्रयोग किया है।
जैसे कबीर दास ने अपनी रचना में सद्दू ककड़ी भाषा का प्रयोग किया है, वहीं तुलसीदास की रचनाओं में अवधि व ब्रजभाषा का सम्मेलन देखने को मिलता है।
सूरदास की रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग दिखता है, वहीं जायसी ने ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग अपनी रचना में किया है।
भक्तिकाल के अन्य नाम
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिए गए इस पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल ही सभी ने स्वीकार किया है। लेकिन इसके अलावा भी हिंदी साहित्य के अन्य लेखकों एवं कवियों ने इसका अलग-अलग नाम दिया है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल कहा है। वहीं श्यामसुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग कहा है। मिश्र बंधु ने इस काल को माध्यमिक काल का नाम दिया है।
FAQ
भक्ति काल के नाम का आधार भक्तित्व है। इस काल में संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं लिखी गई है और उसी के आधार पर इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा है।
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, माध्यमिक काल, स्वर्ण युग और स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अलग-अलग कवियों ने नाम दिया है।
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, जिसकी समयावधि 1350 ईसवी से 1650 ईसवी तक रही है।
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, स्वर्ण युग, स्वर्ण काल और माध्यमिक काल के नाम से जाना जाता है।
भक्ति काल की समयावधि 1350 ईसवी से 1650 ईसवी तक मानी जाती है। लेकिन कुछ विद्वान भक्ति काल का शुभारंभ 1375 ईस्वी मानते हैं।
सोलवीं सदी के महान संत कबीर दास जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, इन्होंने संपूर्ण जीवन वाराणसी में बिताया। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और 1518 ईस्वी में इसी स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। हालांकि मगहर को अपवित्र माना जाता था लेकिन यहां पर संत कबीर दास की मृत्यु ने इस स्थान को पवित्र बना दिया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों के अनुसार भक्ति काल का प्रारंभ 1350 ईसवी से हुआ है। वहीं कुछ विद्वान 1375 से भक्ति काल का शुभारंभ मानते हैं।
निष्कर्ष
इस लेख में आपने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाने वाला भक्ति काल के बारे में सब कुछ जाना।
भक्ति काल वह दौर जिस समय मुस्लिम साम्राज्य के कारण लोगों के अंदर से भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आस्था कम होने लगी थी।
ऐसे हालात में हमारे प्रमुख संत एवं कवियों ने अपने ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग के जरिए लोगों में दोबारा भगवान के प्रति प्रेम, आस्था और श्रद्धा का जागरण किया।
यहां भक्ति काल क्या है (bhakti kaal kya hai), भक्ति काल किसे कहते हैं, भक्ति काल की परिभाषा, भक्ति काल का नामकरण, भक्तिकाल के कवि, भक्तिकाल का विभाजन, भक्ति काल की शाखाएं, भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल का समय आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है।
हमें उम्मीद है कि इस लेख में आपको भक्ति काल से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि यह लेख आपको पसंद आया हो तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें।
यह भी पढ़े
मनोविज्ञान क्या होता है? इसकी शाखाएं और इतिहास
कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है?
संस्कृत भाषा का महत्व और संस्कृत की उत्पत्ति
साइकोलॉजी क्या है?, अर्थ, परिभाषा और शाखाएं