Shikshan Kya Hai: हम मनुष्य किसी न किसी तरीके से कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं होता जीवन में हम अपनी गलतियों से या किसी के सुझाव से जो भी सीखते हैं, वह हर चीज शिक्षण कहलाता है।
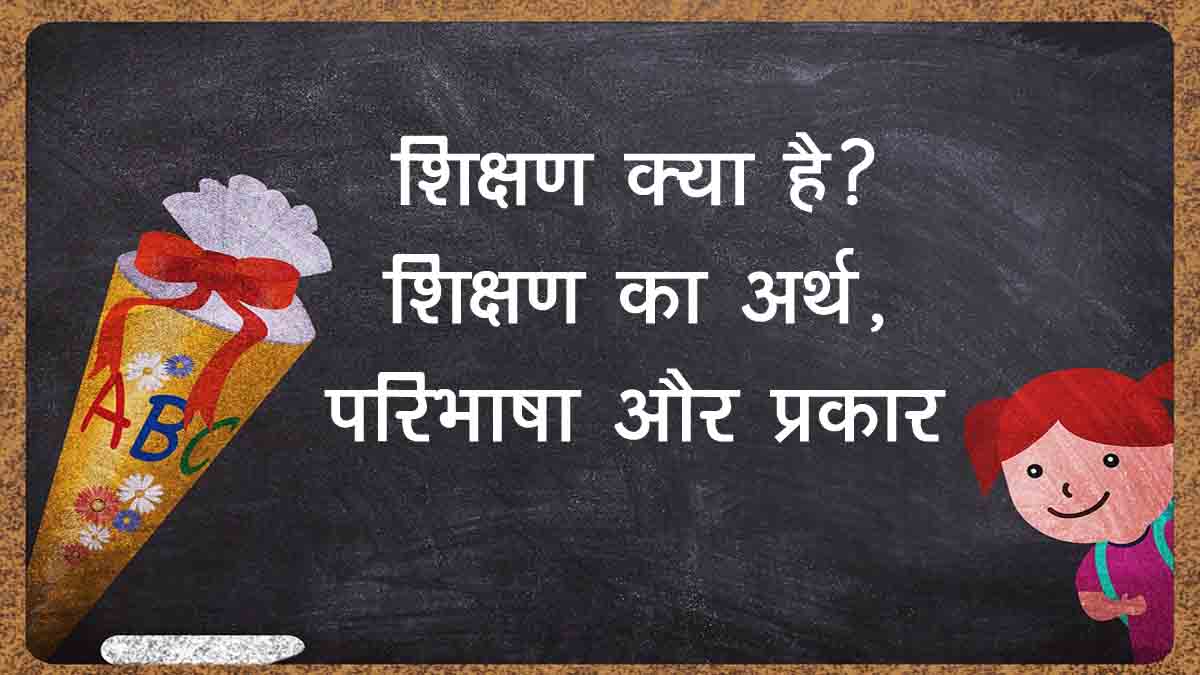
क्या आपको पता है कि इस छोटे से शब्द का एक गहरा अर्थ है। इसके कई प्रकार भी हैं और इसका निश्चित उद्देश्य भी होता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो लेख शिक्षण क्या है?, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning of Teaching in Hindi) को अंत तक जरूर पढ़ें।
शिक्षण क्या है?, शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और प्रकार | Shikshan Kya Hai
शिक्षण का अर्थ (Meaning of Teaching in Hindi)
शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, ज्ञान देना। यह शिक्षा धातु से बना हुआ है। यह एक त्रियामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल है। इन तीनों के बीच आपस में संबंध स्थापित करना ही शिक्षण होता है। अर्थात शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करता है, इसी प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग कहा जाता है।
यदि बात करें शिक्षण का संकुचित अर्थ की तो इसका संबंध स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक छात्रों को एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित स्थान पर बिठा कर निश्चित समय में उसे पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देता है और परामर्श देता है।
वहीँ शिक्षण का व्यापक अर्थ समझे तो उसका अर्थ होगा कि एक व्यक्ति औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से जीवन भर जो भी कुछ सीखता है, वह व्यापक शिक्षण का अर्थ होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बाल केंद्रित शिक्षण दिया जाता है क्योंकि वर्तमान में छात्रों को शिक्षा उनके रुचि के आधार पर दिया जाता है।
हालांकि प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित था, जिसमें बालक के रुचि-अरुचि को बिना महत्व दिए शिक्षा दिया जाता था। इस तरह सरल भाषा में शिक्षण का परिभाषा होता है बालक के अंदर निहित शक्तियों को विकसित करना। एक सही शिक्षा मनुष्य और समाज दोनों का निर्माण करता है और दोनों का साथ में विकास होता है।
शिक्षण के प्रकार
शिक्षण के मूलतः तीन प्रकार हैं:
- तंत्रआत्मक
- लोकतंत्रात्मक
- स्वतंत्रआत्मक
तंत्रात्मक शिक्षण
इस शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का स्थान उच्च होता है। इसमें शिक्षक को प्रधानता दी जाती है, वहीं छात्र का स्थान गौण होता है। इसमें शिक्षक अपने अनुसार छात्र को मार्गदर्शीत करता है। इसमें शिक्षक का आज्ञा का पालन छात्र को करना होता है।
हालांकि इसमें शिक्षक के द्वारा छात्रों को गलत शिक्षा भी दी जा सकती है। क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली में बालक को शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान पर तर्क वितर्क करने का अधिकार नहीं होता। उसका कर्तव्य बस अपने शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षण को ग्रहण करना ही होता है और उसे अपने जीवन में लागू करना होता है।
लोकतंत्रात्मक शिक्षण
लोकतंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों की ही भूमिका होती है। इसमें छात्र शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान पर तर्क वितर्क कर सकता है। इसमें शिक्षक को छात्र के विचारों का भी सम्मान करना पड़ता है।
प्राचीन काल मैं दी जाती शिक्षा एक लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली थी, जिसमें शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षा पर विचार करना उस पर प्रश्न करना बालक का अधिकार था और शिक्षक का कर्तव्य भी था कि वह बालक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे ताकि वह कभी भी किसी बात को लेकर असमंजस में ना रहे।
हालांकि आधुनिक शिक्षण प्रणाली को भी हम कुछ हद तक लोकतंत्रात्मक शिक्षण कह सकते हैं। क्योंकि इसमें बालक पाठ्यक्रम के विषयों पर तर्क वितर्क कर सकता है और मन में उत्पन्न प्रश्न को जानने की इच्छा प्रकट कर सकता है। इस तरह कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक और बालक दोनों ही एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं।
स्वतंत्रात्मक शिक्षण
स्वतंत्रात्मक शिक्षण नवीन शिक्षण पर आधारित है, जिसमें शिक्षक छात्र के साथ मित्र की तरह व्यवहार करता है और इसमें छात्र बिना दबाव में आकर सीखता है। इसमें छात्रों के रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है।
आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रात्मक शिक्षण पर आधारित है, जिसमें बालक को पूरा अधिकार है कि वह अपनी रूचि के अनुसार किसी भी विशेष विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चाहे तो वह अपनी रूचियों को बढ़ा सकता है और आज की शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य बालकों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना ही है।
इस शिक्षा प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता है। हालांकि इसमें भी बालक और शिक्षक एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं।
यह भी पढ़े: जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार
हम सब जानते हैं कि शिक्षण का अर्थ शिक्षा देना होता है। परंतु शिक्षण तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसे सही ढंग से ना दिया जा सके। इसीलिए एक शिक्षक को शिक्षण के सिद्धांत से परिचित होना चाहिए ताकि वह शिक्षण के उद्देश्य को पूरा कर सकें। शिक्षण के सिद्धांत कुछ निम्नलिखित हैं:
- प्रेरणा का सिद्धांत
- रुचि का सिद्धांत
- निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत
- जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत
- नियोजन का सिद्धांत
- चयन का सिद्धांत
- अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत
- क्रियाओ का सिद्धांत
- विभाजन का सिद्धांत
प्रेरणा का सिद्धांत
जब हमसे कोई कहता है कि हम यह काम नहीं कर सकते तब हमारे मन में नकारात्मक भाव आती है कि हम शायद यह नहीं कर सकते, जिससे हम प्रयास तक नहीं करते। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है और कहता है कि हम यह कर सकते हैं तो हमारे अंदर यह कार्य करने की क्षमता है तो स्वयं से हमारे अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है, जो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
भले ही व्यक्ति उस कार्य में सक्षम ना हो लेकिन अपने प्रति प्रशंसा सुनकर व्यक्ति में उस कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा कहा जाता है।
एक सही शिक्षण को चाहिए कि वह प्रेरणात्मक तत्व इस्तेमाल करके बालकों में रुचि उत्पन्न करें। अभी के आधुनिक शिक्षण विधि में प्रेरणा को बहुत महत्व दिया जाता है। बालक में एक बार प्रेरणा संचार हो जाने पर वह पाठ्य को सीखने के लिए शीघ्र ही प्रयास करने लगता है। इस तरह प्रेरणा समस्त प्रकार के शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु है।
रूचि का सिद्धांत
बालक की जिस विषय में रुचि होती है, वह उस विषय को बहुत आसानी से सीख लेता है और समझ लेता है। इसीलिए एक कुशल शिक्षक शिक्षण विधियों को निर्धारित करने से पहले बालकों के रुचि को काफी महत्व देता है।
रुचि के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को पट्ठनिया, स्पष्ट और रुचि पूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक पाठ में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि उसके प्रति बालक में रुचि उत्पन्न हो और वह तन्मय होकर उस चीज को सीखें।
इस प्रकार अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए रुचि का सिद्धांत बहुत मायने रखता है। शिक्षक को पहले छात्र के रुचि के बारे में जानना चाहिए और उस रूचि के विकास पर कार्य करना चाहिए। एक बार रुचि विकसित हो जाएगी तो छात्र स्वयं ही ज्ञान को अर्जन करने में लग जाएगा।
इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक किसी भी विषय को सरल से कठिन के क्रम में प्रस्तुत करें ताकि बालक एक बार जब उस विषयवस्तु को समझने में सफलता मिल जाएगी तो वह सफलता उस बालक को संतोष देगी और वह संतोष बालक में उस विषय के प्रति रुचि जागृत करेंगा।
निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत
उद्देश्य शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कोई भी मनुष्य एक निश्चित उद्देश्य से ही कोई कार्य करता है। उद्देश्य के प्रति उस व्यक्ति की जितनी निष्ठा और समर्पण भाव होती है, वह उस उद्देश्य को पाने के लिए उतना ही ज्यादा मेहनत और प्रयास करता है।
ठीक उसी तरह शिक्षक का छात्रों को शिक्षण देने के पीछे उद्देश्य होता है, उनके पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना। उद्देश्य जितना ज्यादा स्पष्ट होगा उतना ही ज्यादा प्रेरणादायक होगा। व्यक्ति उद्देश्य बनाकर किसी कार्य को शुरू करता है और कार्य उस उद्देश्य को प्राप्त करने तक चलता रहता है।
कार्य का उद्देश्य पता हो तो व्यक्ति निष्ठा से उसको पाने के लिए प्रयास करता है। इस तरह शिक्षण का उद्देश्य होना जरूरी है ताकि बालक उतने ही निष्ठा से शिक्षा प्राप्त करें।
इस प्रकार का सकते हैं कि बिना उद्देश्य के शिक्षक नाभि के समान है, जिसे अपने गंतव्य स्थान का पता नहीं और उद्देश्य के अभाव में छात्र उस पतवारविहीन नाव के समान बन जाता है, जो लहरों के थपेड़े खाते हुए कहीं भी किनारे में लग जाता है। इसीलिए उद्देश्य निश्चित होना बहुत जरूरी है, यह शिक्षण प्रणाली को दिशा प्रदान करता है।
जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत
शिक्षा जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ सीखता है और हर चीज उसके जीवन से संबंध रखता है। ऐसे में शिक्षा एक शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है तो शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बालक को जो भी पढाएं, वह उस विषय से तथ्य और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे, जो बालक के जीवन के कार्यों से जुड़ सके।
इससे प्राप्त ज्ञान से बालक को जीवन में आने वाली कई समस्याओं को सुलझाने में उसे मदद मिलेगी। इसीलिए सभी नवीन शिक्षण प्रणाली में जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत का पूर्ण रुप से पालन किया जाता है।
नियोजन का सिद्धांत
योजना बनाकर शिक्षक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा बालकों को सही से समझ में आता है। इससे शिक्षक को भी समझ में आता है कि उन्हें किस क्रम में प्रस्तुतीकरण करना है ताकि बालक भ्रमित ना हो और उसे क्रम के अनुसार हर चीजें समझ में आती रहे।
इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में जो भी पढ़ाए उसकी पहले से ही क्रमबद्ध योजना बना लें। योजना सही से बना रहेगा तो शिक्षण का उद्देश्य भी समय पर पूरा हो जाएगा।
चयन का सिद्धांत
शिक्षण में चयन का सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि विषय सामग्री सही से चयन ना किया जाए तो उसका पढ़ाना निरर्थक है। शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विषय सामग्री में इतनी ही मात्रा का समावेश करें, जिससे शिक्षण का उद्देश्य समय के अंदर सफलतापूर्वक पूरा हो जाए।
इसके अतिरिक्त शिक्षक को शिक्षण सामग्री का चयन इस तरह करना चाहिए कि वह बालक के जीवनपर्यंत उपयोग में आए। शिक्षण बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षक को बहुत सावधानी पूर्वक उचित और उपयोगी तत्वों का ही चयन विषय सामग्री में करना चाहिए। विषय सामग्री में प्रयुक्त तत्व का चयन करते वक्त शिक्षकों को बालकों के रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए।
अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत
वातावरण बालक को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षण प्रणाली में अनुकूल वातावरण और उचित नियंत्रण महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है। बालक जिस स्थान पर पढ रहा है उसके आसपास का वातावरण जितना उचित और अनुकूल होगा, बालक उतनी ही आसानी से शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली शिक्षण को समझ पाएगा।
अनुकूल वातावरण में बालक की मनोदशा सक्रिय हो जाती है, जिससे विषय वस्तु को समझने में उसके लिए आसानी होता है। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा की स्वच्छता, प्रकाश और रोशनदान की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें।
क्रियाओं का सिद्धांत
शिक्षण में क्रियाओं का सिद्धांत बहुत मायने रखता है। कुछ भी सीखने के लिए बालक का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है। भाषण सुनने से और किताब रट लेने से बालक का विकास नहीं होता है। शिक्षण जितना ज्यादा क्रियाशील होगा बालक के लिए उसे समझना उतना ही ज्यादा सरल होगा। क्रियाशीलता के दो प्रकार हैं: मानसिक क्रियाशीलता और शारीरिक क्रियाशिलता।
मनोविज्ञानी के अनुसार बालक अपने स्वभाव से ही क्रियाशील होता है। बालक जितना ज्यादा कुछ ना कुछ करेगा उसे उतना ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए बालक साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे मात्र साइकिल चलाने की जानकारी दे देने से वह साइकिल चलाना नहीं सीख जाएगा, उसे क्रियाशीलता दिखानी होगी।
उसे खुद साइकिल को पकड़ना, पेंडल पर पांव रखना सीखना पड़ेगा। वह एक बार दो बार गिरेगा लेकिन उस चीज से वह कुछ ना कुछ सीखेगा और फिर अंत में वह साइकिल चलाना सीख जाएगा।
विभाजन का सिद्धांत
शिक्षण बहुत व्यापक और जठिल प्रणाली है। इसमें एक बार में उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे विभाजन के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा।
शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से विभाजित कर दें और उन विषय को सरल से कठिन की ओर अग्रसर होते हुए बढ़ाएं ताकि बालक को पाठ्यक्रम ज्यादा व्यापक भी ना लगे और सब कुछ समझ में आ जाए। जिस तरह जब हम किसी भाषा का ग्रामर सीखते हैं तो सबसे पहले अक्षर का ज्ञान दिया जाता है और फिर शब्द बनाना और शब्द के बाद वाक्य बनाना सिखाया जाता है।
यह भी पढ़े: पर्यावरण (परिभाषा, विशेषताएँ, प्रकार, संरचना और संघटक)
शिक्षण के उद्देश्य
शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक बालक अपने जीवन पर्यंत हर स्थान पर, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन शिक्षण का अर्थ केवल किसी विषय का ज्ञान लेना ही नहीं होता अपितु शिक्षण के कई सारे उद्देश्य हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बालक के अंदर अंतर्निहित शक्तियों से उसे परिचित कराना और शक्तियों को पहचान कर बालक को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना।
- एक अबोध बालक को ज्ञानी बनाना ताकि वह अपने ज्ञान के बल पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हल कर सके।
- बालक में आत्मविश्वास जगाना।
- बालक को सहयोग से रहना सिखाना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसे चाहिए कि वह एक दूसरे के साथ सहयोग से रहे ताकी जीवन को आनंद पूर्वक जिया जा सके।
- बालक के रुचियों का विकास करना।
- बालक को क्रियाशील बनाना ताकि वह मेहनत करने से कभी ना घबराए।
- बालक को प्रेरित करना। बालक प्रेरित होगा तभी उसमें किसी विषय के प्रति रुचि जागृत होगी।
- बालक को जीवन के हर एक पहलू से परिचित कराना ताकि जीवन में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से वो डरे ना।
निष्कर्ष
आज के लेख में हमने आपको शिक्षण क्या है (Shikshan Kya Hai), शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा (Shikshan ka Arth), शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण के प्रकार (Shikshan Ke Prakar) और शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि इस लेख से आप शिक्षण के सही अर्थ से अवगत हुए होंगे।
यदि लेख अच्छा लगा हो तो इसे अपनी सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लेख से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
यह भी पढ़े
कंप्यूटर क्या है तथा इसकी बेसिक जानकारी
आयुर्वेद का इतिहास, महत्व और लाभ
सोशल मीडिया क्या है? इसके प्रकार, फायदे और नुकसान
जीवन बदलने वाली 20 सर्वश्रेष्ठ प्रेरक किताबें