ल्हासा की ओर पाठ का सार (कक्षा 9) | Lhasa Ki Aur Summary
Lhasa Ki Aur Summary: ल्हासा की ओर नामक पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन है, मुख्यत इस पाठ में यात्रा का वृतांत लिखा गया है, राहुल जी यानि हमारे पाठ के लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन इस पाठ में किया है। लेखक की यात्रा का समय 1929 से 1930 तक है।
उस समय जब भारत पर अंग्रेजो का राज था तब किसी भारतीय को तिब्बत यात्रा में जाने पर मनाही थी। इसीलिए लेखक ने यह यात्रा नेपाल के रास्ते की थी, जिसके लिए लेखक को अपना वेश तक बदलना पड़ा था। उन्होंने छद्म रूप धारण किया, एक भिखारी बनकर तिब्बत की यात्रा प्रारंभ की।
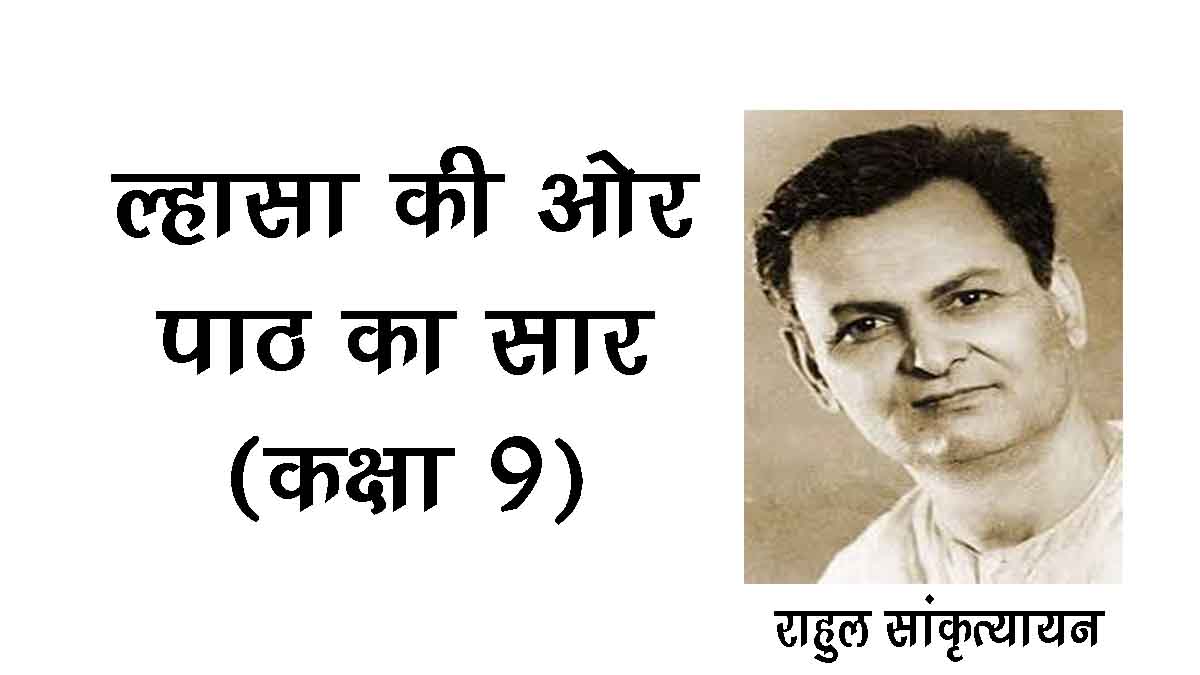
यह यात्रा उस समय की है जब फटी कलिंपोंग का रास्ता बनकर तैयार नहीं था। उन दिनों नेपाल से तिब्बत पहुँचने का केवल एक ही रास्ता हुआ करता था। लेकिन यह रास्ता भी प्रमुख रूप से व्यापार और सैनिकों के प्रयोग में आता था। लेकिन नेपाली और भारतीय भी इसी रास्ते का प्रयोग करते थे आने -जाने के लिए। लेखक के अनुसार उन दिनों यही मुख्य रास्ता हुआ करता था।
आगे पाठ के लेखक बताते है कि उन रास्तों पर जगह जगह चीन देश के फ़ौज की चौकी और किलो की घेराबंदी थी, जो उनका निवास स्थान हुआ करता था। इस समय तो वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके है बिलकुल खंडहर हो चुके है लेकिन
किले के कुछ भागों पर किसानों का बसेरा है। इसीलिए बसेरे वाले भाग अभी भी आबाद है।
ऐसे ही वह एक चीनी किला था जो वीरान हो चुका था, जिसके भागों को ऐसे ही छोर दिया गया गया था। वहां पर लेखक अपने मित्र के साथ चाय अथवा जलपान के लिए थोड़ी देर वहां रुके। उस समय वहा की स्थिति देखकर लेखक ने अंदाज़ा लगाया कि तिब्बत में वहां के निवासियों में ऊंच-नीच, जाति पति, छुआछुत जैसे कोई भावना नहीं थी और न ही वहां की स्त्रिया पर्दानशीं थी।
हाँ, वहां चोरों से जरुर डर था इसीलिए जो निचले स्तर के मामूली भिखारी होते थे, उन्हें घर के अन्दर आने जाने की इजाजत बिलकुल भी नहीं थी। मगर यदि कोई अंजान व्यक्ति वहां है तो उसके लिए कोई प्रतिबन्ध ना था। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति घर की महिलाओं को चाय बनाने का सामान उपलब्ध कराये तो घर में मौजूद महिला उन्हें चाय बनाकर पिलाती थी, वहां की चाय में माखन और नमक डाली जाती थी।
उस त्यागे हुए किले में अपने मित्र के साथ चाय का मजा लेने के बाद जब लेखक आगे बढ़ने लगे। तब वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन दोनों से दो पर्चियों की मांग की। इन पर्चियों को गाँव का पुल पार करने के लिए उन्हें देना ही होता था।
जब वे पुल पार हो चुके थे, उसके बाद ही तुरंत वे थोडला के पूर्व में पड़ने वाले अंतिम गाँव में प्रवेश कर चुके थे।
यहाँ लेखक अपने एक पुराने मित्र सुमति से मिले। सुमति अब बौद्ध भिक्षु है, लेखक के भिखारी वेश में होने के कारण भी उन्हें मित्र की सहायता से रहने के लिए अच्छी जगह मिल गयी। यहां लेखक इस बात का उल्लेख करते है कि जब
वह 5 वर्ष के पश्चात इन्ही रास्तों से वापसी कर रहे थे तब उन्हें जब रहने योग्य स्थान नहीं मिला तो उन्हें कुछ समय के लिए झोपड़ी में रहना पड़ा था। हालाँकि लेखक याद करते हुए बताते है कि उस समय उनका वेश भिखारियों वाला नहीं था। वे उस समय अच्छे यात्री का वेश धारण किये हुए थे।
अब इस यात्रा में लेखक का अगला पड़ाव डाँडा (पहाड़) थोङ्ला था, जिसे पार करना यात्रा का कठिन हिस्सा था। क्योंकि डाँडा तिब्बत में खतरनाक जगह थी, इस तिब्बत की ऊंचाई 1600 से 1700 फीट थी इतनी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण यहां किसी गाँव का कोई नामोनिशान ही नहीं था। यह स्थान डाकुओं के लिए अच्छा था। उनके छिपने के लिए ये काफी उपयुक्त स्थान था और इस मामले में तो सरकार की ओर से भी लापरवाही बरती जाती थी। इसीलिए यहां हत्या लूटपाट होना आम बात थी।
लेखक कुछ हद तक निश्चिंत थे क्योंकि उनका पहनावा भिखारियों वाला था लेकिन हथियारों पर कानून ना लागू होने के कारण थोडा डरना तो लाजमी है। यहां लोग स्वयं की सुरक्षा में हथियारों को अपने घरो में रखा करते थे।
थोङ्ला पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, इसीलिए इस दुर्गम पहाड़ पर जाना बहुत असंभव सा प्रतीत होता था। उसके आगे का स्थान लङ्कोर नामक स्थान था जो वहां से लगभग 16 -17 मील दूर स्थित था। इस कारण दूसरे दिन लेखक उन्होंने अपने मित्र सुमति के साथ डाँडे की ओर चले और वहां की चढ़ाई में उन्होंने घोड़े की सहायता ली। जब वे पहाड़ियों के सबसे उच्च शिखर पर पहुंचे तब उन्होंने देखा दक्षिण पूर्व की ओर नंगे पहाड़ दिख रहे है। उन पर कोई बर्फ कोई हरियाली नहीं है लेकिन यदि उत्तर दिशा में देखे तो कुछ बर्फ दिखायी पड़ रहे थे। उस स्थान पर एक मंदिर था, जो वहां के स्थानीय देवता का था।
पहाड़ों से उतरते समय लेखक एक छोटी सी घटना का जिक्र करते है और बताते है कि उतरते समय उनका घोड़ा थोड़ा धीरे-धीरे चलने लगा था, जिसके कारण उनके सभी साथी आगे निकल गये और वे स्वयं गलत रास्ते की ओर बढ़ गए। करीब डेढ़ मील आगे जाने के बाद उन्हें पता लगा कि वे गलत रास्ते पर है।
बाद में स्थानीय लोगों से संपर्क करने के बाद वे सही रास्ते (लङ्कोर का रास्ता दाहिने के तरफ) वापस आ सके। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनके मित्र सुमति भी उनसे गुस्सा हो गये। आखिर सुमति को उनकी चिंता थी लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मित्र को मना लिया और वे सभी लङ्कोर की एक शानदार जगह पर रुके।
उसके बाद अगली सुबह उनका पड़ाव तिङ्ऱी के मैदान था। तिङ्ऱी के मैदान की यह विशेषता थी कि यह पहाड़ो से घिरा एक टापू था। ठीक इसी के सामने नाम तिङ्ऱी–समाधि–गिरी नाम की छोटी सी पहाड़ी भी वहीं स्थित थी। वहां सुमित की जान पहचान के बहुत सारे लोग भी मिल गये।
सुमति उनसे मिलना और उन्हें बोध गया से लाये कपड़ों के गंडे भेंट स्वरुप देना चाहते थे। लेकिन लेखक यहां अपना समय नहीं गवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुमति को मना कर दिया और वादा किया कि ल्हासा पहुंचकर वे उन्हें पैसे दे देंगे। सुमति ने भी इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब लेखक और उनके साथी आगे की ओर बढ़ने लगे।
अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने सुबह नहीं की इसीलिए चलते समय उन्हें कड़कती धूप का सामना करना पड़ रहा था, जब सामान उठाने के लिए कोई कुली नहीं मिला तब वे सभी अपना अपना सामान उठाकर हाथ में डंडा लिए आगे बढ़ते गये। सुमति यहां एक बार फिर से किसी यजमान से भेंट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहाना बनाया और सभी को टोकर विहार की ओर प्रस्थान करने को कहा।
तिब्बत की जमीनों पर जागीरदारों का अधिपत्य था। सभी छोटे-बड़े जागीरदारों के हाथों में जमीने थी, बौद्ध मठ में भी इन्ही जागीरो से बड़ा हिस्सा सदैव जाता था। जागीरदार खेती का कार्य स्वयं देखते थे और मजदूरों का प्रबंध तो बेगार
व्यक्तियों से हो ही जाता, वहां जो निवासी बौद्ध भिक्षु थे वे खेतो पर निगरानी रखते थे।
उसी स्थान पर लेखक की मुलाकात शक्कर की खेती करने वाले मुखिया से हुई जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे हुई न्मसे का जो मठ था, उसमें एक सुन्दर मंदिर भी था। वहां पर भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियों का संग्रह था। लेखक तुरंत ही उसे उलट पलट कर देखने लगे और पढने लगे।
लेखक को सुमति ने व्यस्त देखकर उनसे पूछा कि क्या वे आस पास के यजमानो से मिल आये। जिस पर लेखक ने अपनी स्वीकृति दे दी। दोपहर तक सुमति अपने सभी यजमानो से भेंट कर वापस लौट आये। अब वहां से तिङ्ऱी बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर लादा और न्मसे से विदाई ली और आगे की ओर बढ़ चले।
राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय
ल्हासा की ओर (Lhasa Ki Aur Summary) नामक यात्रा वृतांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म स्थान उनका ननिहाल था। सन 1893 में पन्दाह गाँव में जन्मे राहुल जी का मूल नाम केदार पाण्डेय था, पन्दाह गाँव अब उत्तर प्रदेश केआजमगढ़ जिले में है।
उनके पिता का नाम श्री गोवर्धन पाण्डेय था जो कनैला (आजमगढ़) के निवासी थे।
उनके बचपन का अधिकतर समय ननिहाल में ही बीता। नाना रामशरण पाठक एक फौजी रह चुके थे और नौकरी के दौरान उन्होंने दिल्ली, नासिक, अमरावती आदि शहर देखे थे तो अपने नाना से उनकी यात्रा की कहानियां सुन सुनकर बालक केदार बड़े हुए। इन कहानियों को सुनने के दौरान ही उनके मन में विश्व भ्रमण की लालसा जगी।
इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी और आगरा से हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर चले गये इन्होने इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और अन्य भाषाओं में भी पांडित्य प्राप्त की। वे स्वदेश ही नहीं बल्कि विदेशों जैसे नेपाल, कोरिया, ईरान, चीन में भी खुद घूमे। हालाँकि इन यात्राओं का पूर्ण उल्लेख कम ही है। सन 1963 में राहुल जी का देहांत हो गया।
इनकी साहित्यिक कृतिया निम्न है:
कहानियाँ: वोल्गा से गंगा, कनैला की कथा, सतमी के बच्चे
आत्मकथा: मेरी जीवन यात्रा, जिसके कुल 6 भाग है
उपन्यास: जीने के लिए, सिंह सेनापति, भागो नहीं, दुनिया बदलो, दिवोदास, विस्मृत यात्री
जीवनी: सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियाँ, लेनिन, कार्ल मार्क्स, घुमक्कड़ स्वामी, जिनका मै कृतज्ञ, जयवर्धन, कप्तान लाल
यात्रा साहित्य: लंका, जापान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, रूस में पच्चीस मास, मेरी लद्दाख यात्रा
यह भी पढ़े
- बालगोबिन भगत पाठ का सार (कक्षा 10)
- बालगोबिन भगत पाठ के प्रश्न उत्तर (कक्षा 10)
- कन्यादान कविता का सार और भावार्थ
- राम लक्ष्मण परशुराम संवाद
- “साना साना हाथ जोड़ि” पाठ का सार